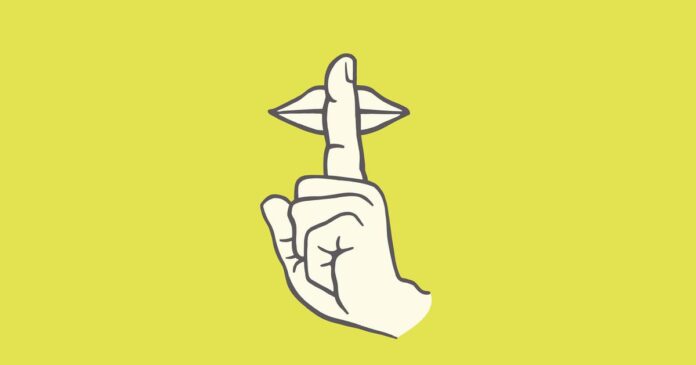संस्कृति में विनिवेश
पहले की किसी सरकार के मुक़ाबले वर्तमान सरकार संस्कृति की ओर ध्यान देने का बार-बार दावा करती रही है. उसने संस्कृति के क्षेत्र में बहुत भव्य और खर्चीले उत्सव भी आयोजित किये हैं जिन्हें राजनीतिक तमाशों के रूप में भी देखा-समझा गया. गंगा आरती, कुम्भ आदि जो मूलतः धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन हैं अब राजनैतिक प्रक्षेपण और लाभ के लिए बहुत चमक-दमक के साथ किये जाने लगे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अब स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार के थिंक टैंक की तरह सक्रिय है, अपने को दशकों से एक सांस्कृतिक संगठन कहता आया है.
संस्कृति के लिए यह मुखर सरोकार क्या वर्तमान सरकार द्वारा उसके लिए किये जा रहे वित्तीय निवेश में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है? अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट आंकड़े सामने आये हैं उनके अनुसार संस्कृति मंत्रालय के लिए कुल प्रावधान 2687.99 करोड़ का है जो भारत सरकार के कुल बजट का 0.08 प्रतिशत है याने एक प्रतिशत के दसवें हिस्से से भी कम. यह नोट करना दिलचस्प है कि वर्ष 2020-21 के बजट में संस्कृति के लिए प्रावधान 3150 करोड़ का था जो कि कुल बजट का लगभग 0.1 प्रतिशत था. अगले वित्तीय वर्ष में यह प्रावधान कुल राशि और प्रतिशत दोनों में कम हो गया है. इस कटौती का प्रतिकूल प्रभाव गतिविधियों पर ही पड़ेगा क्योंकि स्थापना पर खर्च तो कम नहीं किया जा सकेगा.
संस्कृति के लिए प्रावधान सभी सरकारों में कम रहा है. दशकों पहले जब राष्ट्रीय संस्कृति नीति का एक मसविदा तैयार करने की हमने कोशिश की थी तो इस प्रतिशत को क्रमशः बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था. यह पिछली सदी के अन्त के क़रीब की बात है: दो दशकों से अधिक समय बीत चुका और वित्तीय विनिवेश धीरे-धीरे ही रेंग रहा है. यह नोट करना दिलचस्प है कि सत्तामूलक राजनीति में सभी दलों के बीच इस पर अलिखित-अघोषित सहमति है कि संस्कृति में विनिवेश करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है.
सरकार के अन्तर्गत जो स्वायत्त संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय अकादेमियां आदि हैं उन पर आने-वाले ख़र्च का एक बढ़ा हिस्सा वेतन-भत्तों याने स्थापना पर होता है. उनके पास गतिविधियों के लिए बहुत कम राशि बचती है. इन संस्थाओं का काम-धाम अक्सर तरह-तरह के वफ़ादार मीडियोकरों के हाथों में होने के कारण किसी तरह की नयी पहल या नवाचार संभव ही नहीं हो पाता. बड़ी विडम्बना है कि विशेषतः युवाओं के अलग समूह तरह-तरह से निर्भीक नवाचार कर रहे हैं लेकिन सरकारी सहायता से चलने वाली संस्थाओं में उसकी कोई भनक तक नहीं है. जैसे लोकतंत्र को अपने को सशक्त और सार्थक रखने के लिए नवाचार चाहिये वैसे ही संस्कृति को भी. निरे पिष्टपेषण से संस्कृति आगे नहीं बढ़ती. यों उसे आगे बढ़ाने का, कम से कम, सरकार में कोई इरादा भी नहीं है.
आलोचना पर दुलत्तियां
हिन्दी में आलोचना एक ऐसी विधा है जिस पर आये दिन कोई न कोई एक दुलत्ती लगा देता है. यह दिलचस्प है कि सभी उससे असन्तुष्ट रहते हैं, यहां तक कि स्वयं आलोचक भी, पर हरेक को उसकी दरकार भी रहती है. रचनाकार भले कभी-कभार सार्वजनिक रूप से ऐसे वक्तव्य देते हों जिनमें कहा गया होता है कि उन्हें आलोचना की रत्ती भर परवाह नहीं है पर अकसर उन्हें, अन्दर-ही-अन्दर, उपयुक्त आलोचना की दरकार रहती है. कई बार आलोचना की रीतिबद्धता का ज़िक्र होता है पर प्रचलित रूढ़ियों से अलग रहकर जो आलोचना लिखी गयी है, उसका नोटिस नहीं लिया जाता.
जैसी अख़बारी सम्प्रेषणीयता धीरे-धीरे कविता में प्रतिमान बनती गयी है, वैसी ही सम्प्रेषणीयता आलोचना में भी लगातार अपेक्षित होती गयी है. सोशल मीडिया पर उसी आलोचना की चर्चा होती है जो इसी सम्प्रेषणीयता की वृत्ति का पालन करते हुए लिखी जाती है और जिसे आसानी से प्रशंसा-निन्दा के खानों में डाला जा सकता है. अच्छी आलोचना सिर्फ़ लिखने भर में नहीं पढ़ने-समझने में कुछ जतन, कुछ सावधान और संवेदनशील पाठ की मांग करती है. हमारी अक्सर अतर्कित हड़बड़ी या अधीरता आलोचना को लेकर किसी अध्यवसाय के आड़े आती है. यह कहने का पर्याप्त आधार है कि हिन्दी में साहित्य को पढ़ने-समझने की जो साहित्यिक साक्षरता विकसित हुई है, उसमें अच्छी आलोचना से पायी गयी समझ की कम भूमिका और जगह है.
अगर आलोचना की ऐसी स्थिति है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या कारण है कि ज्ञान के इतने सारे केन्द्रों, विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों, अकादेमियों-संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं के रहते आलोचना लगातार रूढ़ियों-रीतियों में फंसती-उलझती रही है? स्वयं हिन्दी समाज के एक बड़े और पढ़े-लिखे हिस्से में आलोचना-वृत्ति का भयानक क्षरण हुआ है. वह प्रश्नवाचक, लोकतांत्रिक और आलोचना-बुद्धि से लैस होने के बजाय आज्ञापालक, अन्ध भक्त हो गया है जिसमें बहुत आसानी से आलोचना या असहमति को द्रोह माना जाने लगा है. कम से कम हिन्दी समाज और राज में अभूतपूर्व सहमति है कि प्रश्न पूछना, असहमत होना द्रोही होना है. राज माने तो माने, समाज भी ऐसा ही मानने और उसके अनुसार आचरण करने लगा है. राज से पहले अब तो समाज ही ऐसे द्रोह को दण्डित करने के लिए सक्रिय हो जाता है.
यह भी सोचने की बात है कि हमारी ढेर सारी आलोचना कृति-केन्द्रित न होकर विचार-केन्द्रित है. ज़्यादातर विचार स्वयं साहित्य से उपजे या उसमें चरितार्थ विचार नहीं होते. वे अन्यत्र विकसित विचार होते हैं. हमारे लगभग सर्वमान्य मूर्धन्यों पर कितनी आलोचना-पुस्तकें हैं जो हम सहज ही याद कर सकते हैं? हमारी आलोचना ने, दुर्भाग्य से, हमें बड़े लेखकों बड़ी कृतियों को ध्यान और जतन से, समझ और संवेदना से, दृष्टि और प्रश्नाकुलता से पढ़ना-समझना बहुत कम सिखाया है. सोचें कि अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, प्रसाद, महादेवी, निराला, पन्त, रेणु, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, रघुवीर सहाय, श्रीकान्त वर्मा आदि पर कितनी कम पुस्तकें हैं जो हमें इन लेखकों को समझने की राह पर ले जाती हों! कृति-केन्द्रित आलोचना की उपेक्षा का एक उदाहरण वागीश शुक्ल की निराला की ‘राम की शक्तिपूजा’ कविता की टीका ‘छन्द छन्द पर कुमकुम’ है जिसकी चर्चा ही नहीं हुई. याद आता है कि बालचन्द्र राजन की मिल्टन पर पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी तब उनकी आयु शायद 25 बरस की थी. उस पुस्तक के बाद मिल्टन पर असंख्य पुस्तकें लिखी गयी हैं पर उन सबने राजन की पुस्तक को हिसाब में लिया है. हम अक्सर कृतियों के कालजयी होने की बात सोचते हैं, आलोचनात्मक पुस्तकों के कालजयी होने की नहीं. वे भी कालजयी होती हैं. रामचन्द्र शुक्ल का ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, विजयदेव नारायण साही की पुस्तक ‘जायसी’, उदाहरण के लिए, कालजयी पुस्तकें हैं.
रेणु शती
रेणु की जन्म शताब्दी के सिलसिले में दस पत्रिकाओं के विशेषांक प्रकाशित हुए जिनकी अब तक सूचना है. कई और पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले या रेणु पर विशेष सामग्री दी है. मोटा अनुमान यह है कि रेणु के जीवन और कृतित्व पर लगभग 400 नये लेख लिखे गये हैं और उनकी जन्मशती के दिन याने 4 मार्च 2021 को हिन्दी अंचल और उससे बाहर रेणु पर एकाग्र सौ से अधिक आयोजन हुए हैं. हिन्दी साहित्य समाज में रेणु को लेकर यह व्यापक उत्साह कई अर्थों में अभूतपूर्व है और यह ज़ाहिर करता है कि सच्चे और मूल्यवान की जगह और सम्मान हिन्दी जगत् में कम नहीं हुए हैं. यह समूचे साहित्य-समाज के लिए बहुत उत्साहप्रद है. इस सिलसिले में कवि-पत्रकार विमल कुमार की अथक भूमिका भी अत्यन्त प्रशंसनीय है. रेणु-सजगता फैलाने में वे लगातार सक्रिय और मुखर रहे हैं. कई विशेषांक और आयोजन उनके उकसाने से ही सम्भव हुए हैं.